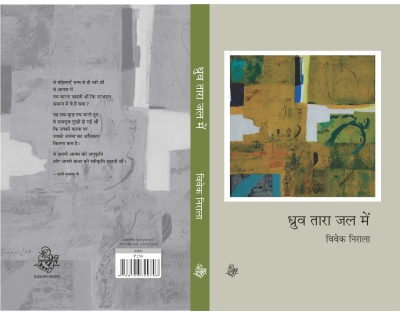|
| रमेश उपाध्याय |
संस्मरण केवल उस विशेष व्यक्ति, जो कि उसका लेखक होता है, की ही आपबीती नहीं होता बल्कि उसमें अपने समय का एक इतिहास भी होता है. कहानीकार और सम्पादक रमेश उपाध्याय के इस संस्मरण से हमें न केवल उस समय के उनके खानाबदोशी के जीवन, रोजगार की जद्दोजहद बल्कि इब्राहीम शरीफ जैसे उम्दा लेखक के व्यक्तित्व के साथ-साथ समान्तर कहानी आन्दोलन और उसके पेचोखम के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं. तो आइए आज पहली बार पर पढ़ते हैं रमेश उपाध्याय का यह महत्वपूर्ण और रोचक संस्मरण ‘इब्राहीम शरीफ : स्वतन्त्र लेखन की चाह का दुखान्त’.
इब्राहीम शरीफ : स्वतन्त्र लेखन की चाह का एक दुखांत
रमेश उपाध्याय
प्रेम की गहराई का सम्बन्ध उसकी अवधि से नहीं होता। लम्बे समय तक प्रेम करने वाले दो व्यक्ति भी कभी यह महसूस कर सकते हैं कि उनके बीच जो था, वह तो प्रेम था ही नहीं। दूसरी तरफ केवल कुछ दिन साथ रह कर भी दो व्यक्तियों में इतना प्रगाढ़ प्रेम हो सकता है कि आजीवन भुलाये न भूले। मित्रता में भी ऐसा ही होता है। इब्राहीम शरीफ का और मेरा साथ तीन-चार वर्षों का ही रहा, पर उस थोड़े-से ही समय में उससे मेरी ऐसी दोस्ती हुई, जो मुझे लगता है कि आज भी कायम है, जब कि उसको गुजरे चार दशक हो चुके हैं।
उम्र में इब्राहीम शरीफ मुझसे पाँच साल बड़ा था। उसका जन्म 1937 में हुआ था और मेरा 1942 में। लेकिन लिखना हमने लगभग साथ-साथ शुरू किया था। हमने 1960 के दशक में कहानी लिखना शुरू किया था, लेकिन ‘साठोत्तरी’ कहलाने वाले कहानीकारों (ज्ञानरंजन, दूध नाथ सिंह, रवींद्र कालिया आदि) के बाद के युवा कहानीकारों में हमारी गिनती होती थी। हिन्दी कहानी में ‘नयी कहानी’ के आन्दोलन के बाद कई कहानी आन्दोलन चले थे, जैसे साठोत्तरी कहानी (1960 के बाद की या सातवें दशक की हिन्दी कहानी), अकहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी आदि। हमारी कहानियाँ इन सब आन्दोलनों से सम्बन्धित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थीं, लेकिन हम इनमें से किसी भी आन्दोलन में शामिल नहीं थे और अपने लेखन से अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे। अतः हमें हमारी उम्र के आधार पर युवा कहानीकार कहा जाता था।
दिसंबर, 1970 में पटना (बिहार) से निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका ‘सिर्फ’ की ओर से एक युवा लेखक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें दूसरे बहुत-से युवा लेखकों के साथ-साथ मुझे भी आमंत्रित किया गया था। उस समय मैं एम. ए. और शादी करने के बाद दिल्ली में रहता था और प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर के अंग्रेजी साप्ताहिक ‘शंकर्स वीकली’ के हिन्दी संस्करण ‘हिन्दी शंकर्स वीकली’ में काम करता था। ‘हिन्दी शंकर्स वीकली’ का प्रकाशन उसी साल शुरू हुआ था। शंकर जवाहर लाल नेहरू के मित्र थे, उन से उनके पारिवारिक सम्बन्ध थे, इसलिए ‘हिन्दी शंकर्स वीकली’ का लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। संयोग से उसके दोनों सम्पादक कथाकार थे और दोनों के नाम रमेश थे। प्रधान सम्पादक थे रमेश बक्षी और सहायक सम्पादक रमेश उपाध्याय। बक्षी जी ‘नयी कहानी’ आन्दोलन से सम्बन्धित वरिष्ठ कथाकार थे, जबकि मैं तब तक किसी भी आन्दोलन से असंबद्ध युवा कथाकार।
पटना में हो रहे युवा लेखक सम्मेलन में मेरा जाना तय था। दिल्ली से जा रहे कुछ अन्य लेखकों के साथ मैंने रेल-आरक्षण भी करा लिया था, लेकिन उसी समय मुझे दिल्ली छोड़ कर बंबई जाना पड़ा। बंबई से एक पत्रिका निकलती थी ‘नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट’, जो अंग्रेजी ‘रीडर्स डाइजेस्ट’ की तर्ज पर निकाली जाती थी। कुछ दिन पहले ‘नवनीत’ के सम्पादक नारायण दत्त बंबई से दिल्ली आये थे। मैं कुछ समय स्वतन्त्र लेखक के रूप में बंबई में रह चुका था और ‘नवनीत’ के लिए कुछ लेखन तथा अनुवाद कर चुका था, इसलिए वे मुझे जानते थे। वे मुझसे मिले। उन्हें ‘नवनीत’ के लिए एक ऐसे सहायक सम्पादक की जरूरत थी, जो सम्पादन के साथ-साथ लेखन और अनुवाद भी कर सके। वे जानते थे कि मैं ‘हिन्दी शंकर्स वीकली’ से पहले ‘सरिता’, ‘मुक्ता’ और ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’ के सम्पादकीय विभागों में काम कर चुका हूँ और ‘धर्मयुग’, ‘सारिका’, ‘कल्पना’, ‘ज्ञानोदय’ आदि प्रसिद्ध पत्रिकाओं में लिखने वाला चर्चित युवा लेखक हूँ। उन्होंने ‘हिन्दी शंकर्स वीकली’ के मुकाबले ड्योढ़े वेतन पर ‘नवनीत’ के सहायक सम्पादक का पद सँभालने के लिए कहा, तो मैं राजी हो गया और पटना के युवा लेखक सम्मेलन में जाने के बजाय ‘नवनीत’ में काम शुरू करने के लिए बंबई चला गया।
‘नवनीत’ का दफ्तर ताडदेव में एक पुरानी इमारत की ऊपरी मंजिल पर था। सहायक सम्पादक होने के नाते मुझे दफ्तर में एक अलग कमरा मिला हुआ था। एक दिन मैं अपने कमरे में अकेला बैठा कुछ काम कर रहा था कि बंबई का मेरा एक युवा कहानीकार मित्र जितेन्द्र भाटिया एक लम्बे, छरहरे, साँवले-से युवक के साथ मुझ से मिलने आया। वह युवक था इब्राहीम शरीफ। व्यक्तिगत रूप में हम पहली बार मिल रहे थे, किन्तु कहानीकार के रूप में हम एक-दूसरे को पहले से जानते और पसन्द करते थे। जितेन्द्र हम दोनों का साझा मित्र और प्रिय कहानीकार था। शरीफ उस समय कालीकट (केरल) के सर सय्यद अहमद कॉलेज में हिन्दी पढ़ाता था (एम.ए. हिन्दी की पढ़ाई उसने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से की थी) और जितेन्द्र बंबई के आइ. आइ. टी. में पढ़ रहा था।
वे दोनों पटना के युवा सम्मेलन से लौटे थे। शरीफ ने मुझसे पूछा, ‘‘आप वहाँ क्यों नहीं आये? मुझे उम्मीद थी कि आप तो वहाँ जरूर मिलेंगे। वहाँ के लोग भी कह रहे थे कि आपका आना निश्चित था। फिर क्या हुआ?’’
मैंने संक्षेप में ‘हिन्दी शंकर्स वीकली’ और दिल्ली छोड़ कर ‘नवनीत’ में बंबई आने का किस्सा सुना कर पूछा, ‘‘पटना में क्या-क्या हुआ?’’
जितेन्द्र और शरीफ वहाँ से बहुत क्षुब्ध हो कर लौटे थे। उन्हें वहाँ पर साहित्यिक राजनीति और लेखकीय गुटबंदियों के कुछ कटु अनुभव हुए थे। दोनों ने विस्तार से अपने अनुभव सुनाये और मुझसे कहा, ‘‘अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए।’’
‘‘क्या?’’ मैंने पूछा।
‘‘हम नये लेखकों को साठोत्तरी लोगों से अलग अपनी पहचान बनानी चाहिए, क्यों कि जिस तरह ‘नयी कहानी’ वालों ने इन लोगों को ‘‘अपना ही विस्तार’’ कहा था, उसी तरह ये भी हम लोगों को ‘‘अपना ही विस्तार’’ कह कर हमारी नवीनता और भिन्नता को नकारना चाहते हैं। हमें यह मंजूर नहीं।’’
मैंने चाय मँगवायी, चाय की चुस्कियों के साथ कुछ हल्की-फुल्की बातें कीं और हँस कर पूछा, ‘‘तो हम लोग भी अपना एक अलग गुट बनायें?’’
शरीफ गुटबंदी की निन्दा कर चुका था, इसलिए थोड़ा अचकचा कर बोला, ‘‘नहीं, गुट तो नहीं, पर…’’
मैं शायद यही सुनना चाहता था। मैंने कहा, ‘‘तब हमें गंभीरता से एक नया कहानी आन्दोलन चलाने के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए पहले हमें एक सूची बनानी चाहिए कि नये लेखकों में से कौन-कौन हमारे साथ आ सकते हैं। फिर यह सोचना चाहिए कि आन्दोलन के जरिये हम करना क्या चाहते हैं। उसी उद्देश्य के मुताबिक हमें आन्दोलन का नाम रखना चाहिए और उसी नाम से एक पत्रिका निकालनी चाहिए, जो हमारे आन्दोलन का मंच बन सके।’’
जितेन्द्र यह सुन कर उछल पड़ा। बोला, ‘‘रमेश, तुम विश्वास नहीं करोगे, पर मैं भी ठीक ऐसा ही कुछ सोच रहा था।’’
‘‘और आप क्या सोचते हैं, शरीफ साहब?’’ मैंने शरीफ से पूछा।
‘‘पहली बात तो यह कि आप मुझे शरीफ साहब नहीं, शरीफ ही कहिए। दूसरी बात यह कि मैं आप दोनों से सहमत हूँ।’’ शरीफ ने मुस्कराते हुए कहा।
‘‘तो शाम को कहीं मिलते हैं और इस पर विस्तार से बात करते हैं।’’ मैंने कहा।
‘‘शाम को हम दोनों कमलेश्वर जी से मिलने ‘सारिका’ के दफ्तर में जायेंगे। चाहो, तो तुम भी वहीं आ जाओ। उनसे मिलने के बाद जहाँ तुम कहोगे, चले चलेंगे।’’ जितेन्द्र ने कहा और मैं राजी हो गया।
कमलेश्वर उन दिनों कहानी पत्रिका ‘सारिका’ के सम्पादक थे और हम नये कहानीकारों की कहानियाँ बड़े प्रेम से छापते थे। मैं उन्हें तब से जानता था, जब वे दिल्ली में ‘नयी कहानियाँ’ पत्रिका के सम्पादक थे। वे उम्र में मुझ से बड़े थे, और बड़े साहित्यकार तो थे ही, फिर भी मुझसे मित्रवत व्यवहार करते थे।
शाम को अपने दफ्तर से मैं उनके दफ्तर पहुँचा, तो मैंने पाया कि जितेन्द्र और शरीफ एक नया कहानी आन्दोलन शुरू करने का विचार उन्हें बता चुके हैं और कमलेश्वर उसी के बारे में कुछ कह रहे हैं। कमलेश्वर ने खड़े हो कर मेरा स्वागत करते हुए कहा, ‘‘आओ, रमेश! हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। नया कहानी आन्दोलन शुरू करने का तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। मैं जितेन्द्र और शरीफ से कह रहा था कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम लोग ‘सारिका’ को अपनी ही पत्रिका समझो और इसी को अपने आन्दोलन का मंच बनाओ।’’
वे लोग चाय पी चुके थे, पर मेरे पहुँचने पर चाय का एक दौर और चला, जिसके दौरान आन्दोलन के नाम पर विचार होने लगा। उन दिनों बंबई की फिल्मी दुनिया में ‘समांतर सिनेमा’ के नाम से एक नया आन्दोलन शुरू हुआ था, जिसके अन्तर्गत बंबइया सिनेमा की व्यावसायिक लीक से हटकर कुछ नये ढंग की फिल्में बनायी जा रही थीं। बातों ही बातों में कमलेश्वर ने कहा, ‘‘समांतर कहानी नाम कैसा रहेगा?’’
‘‘बहुत अच्छा रहेगा।’’ हम तीनों ने खुश हो कर लगभग एक साथ कहा।
‘‘तो मिलाओ हाथ।’’ कमलेश्वर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर जितेन्द्र, शरीफ और मैंने तले-ऊपर अपने हाथ रखे और कमलेश्वर ने दूसरे हाथ से हम तीनों के हाथों को दबाते हुए कहा, ‘‘समांतर कहानी जिन्दाबाद!’’
शरीफ तो शायद अगले दिन अपने घर मद्रास चला गया, पर मैं और जितेन्द्र समांतर कहानी आन्दोलन की शुरुआत के लिए युवा कहानीकारों का एक सम्मेलन बंबई में कराने के काम में उत्साहपूर्वक जुट गये। कमलेश्वर से भी लगातार सलाह-मशविरा होने लगा। बंबई में उस समय जो अन्य युवा कहानीकार थे (जैसे सुदीप, अरविंद, निरुपमा सेवती, राम अरोड़ा आदि), उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क और संवाद किया गया। दूसरी जगहों के लोगों के साथ पत्राचार के जरिये बात की गयी।
अन्ततः जून, 1971 में ‘समांतर’ का पहला सम्मेलन बंबई में हुआ, जिसमें भाग लेने वाले लेखक थे- कमलेश्वर, कामतानाथ, मधुकर सिंह, रमेश उपाध्याय, जितेन्द्र भाटिया, से.रा. यात्री, सुदीप, सतीश जमाली, राम अरोड़ा, दामोदर सदन, अरविंद, निरुपमा सेवती, आशीष सिन्हा, विभु कुमार, श्याम गोविंद, सनत कुमार, मृदुला गर्ग, श्रवण कुमार, प्रभात कुमार त्रिपाठी, शीला रोहेकर आदि।
इब्राहीम शरीफ को भी उस सम्मेलन में आना था, लेकिन किसी कारणवश वह आ नहीं पाया था। उसने अपना लिखित परचा भेजा था, जो एक गोष्ठी में बाकायदा पढ़ा गया था और उस पर चर्चा की गयी थी।
सम्मेलन बहुत सफल रहा था। पूरे हिन्दी जगत में उसकी धूम मची थी और ‘समांतर कहानी’ तुरन्त चर्चा में आ गयी थी। अगले साल 1972 में कमलेश्वर द्वारा सम्पादित ‘समांतर-1’ नामक कहानी संकलन भी प्रकाशित हुआ था, जिसमें सम्मेलन की विस्तृत रपट थी और उसमें भाग लेने वाले लेखकों की कहानियाँ।
समांतर सम्मेलन के बाद शरीफ के दो पत्र मुझे मेरे बंबई के पते पर मिले। उसका पहला पत्र यह था:
54, Bazar Road
Mylapore, Madras-4
19-6-71
प्रिय भाई,
बंबई में दुबारा आपसे मिल नहीं सका, इसका मलाल है। बहरहाल, मैं मद्रास पहुँच तो गया था, लेकिन बहुत चाह कर भी थोड़ी-सी व्यस्तता की वजह से आपको तत्क्षण लिख नहीं सका, क्षमा करेंगे।
बंबई वाली गोष्ठी में आप रहे होंगे। क्या कुछ हुआ वहाँ, लिखने की कृपा करेंगे।
मैंने जिस योजना की बात आपसे कही थी, उस सम्बन्ध में निवेदन है कि यथाशीघ्र सुदीप का अन्तरंग परिचय भेजें। साथ ही आपके पास अपनी कहानी ‘पुराने जूतों की जोड़ी’ की कटिंग हो तो भेजें, अपने चित्र के साथ। एक बात और, अपनी इस कहानी को ले कर 500 शब्दों का एक वक्तव्य भी भेजें। यह सब जितना जल्द मिल जाये उतना सुविधाजनक रहेगा मेरे लिए।
और? संभव हुआ तो मैं अगले महीने आपके लिए कोई कहानी भेजूँगा।
सानंद होंगे।
पत्र दीजिएगा।
आपका
इब्राहीम शरीफ
शरीफ के पहले पत्र में जिस योजना का जिक्र है, वह यह थी कि मद्रास से निकलने वाली पत्रिका ‘अंकन’ में शरीफ एक स्थायी स्तंभ शुरू करेगा, जिसमें वह हर बार किसी युवा कहानीकार की एक कहानी, कहानी से सम्बन्धित एक लेखकीय वक्तव्य और किसी अन्य कहानीकार द्वारा लिखा गया उसका अन्तरंग परिचय दिया करेगा। बंबई में हुई पहली मुलाकात में ही उसने अपनी यह योजना मुझे बतायी थी। स्तंभ की शुरुआत वह सुदीप से करना चाहता था। सुदीप मेरा मित्र था, इसलिए उसका अन्तरंग परिचय शरीफ मुझसे लिखवाना चाहता था। उस स्तंभ के लिए मेरी कहानी ‘पुराने जूतों की जोड़ी’ उसने पहले से ही चुन रखी थी। मेरा अन्तरंग परिचय वह सुदीप से लिखवाना चाहता था। शायद उसकी योजना यह थी कि दो कहानीकार मित्र एक-दूसरे का अन्तरंग परिचय लिखें।
‘‘अगले महीने आपके लिए कोई कहानी भेजूँगा’’ का सन्दर्भ यह है कि मैंने ‘नवनीत’ में प्रकाशित करने के लिए उससे कहानी माँगी थी।
बंबई में मुझसे हुई पहली मुलाकात होने तक वह कालीकट के कॉलेज की नौकरी छोड़कर मद्रास आ चुका था और मद्रास में अपना प्रेस लगा कर आजीविका की समस्या के स्थायी समाधान के बारे में सोच रहा था। प्रेस लगाने के बाद एक पत्रिका निकालने और पुस्तकों का प्रकाशन करने की भी उसकी योजना थी, जिसकी चर्चा उसने मुझसे और जितेन्द्र से की थी। हम दोनों ने खुश हो कर उसका उत्साह बढ़ाया था। अतः उसके पहले पत्र का उत्तर लिखते समय मैंने ‘नवनीत’ के लिए उसकी कहानी फिर से माँगी थी और प्रेस के बारे में पूछा था। मेरे उस पत्र के उत्तर में उसने लिखा था:
54, Bazar Road
Mylapore, Madras-4
5-7-71
प्रिय भाई,
आपका पत्र मिल गया था। उत्तर देने में देरी हुई। क्षमा करेंगे।
गोष्ठी के बारे में बहुत विस्तार से जितेन्द्र ने लिखा है। जानकर बहुत खुशी हुई कि गोष्ठी हर दृष्टि से सफल रही।
अब तक कहानी, वक्तव्य और चित्र नहीं मिला है। कृपया जल्द भिजवा दीजिए।
अन्तरंग परिचय के बारे में आपने जो लिखा है, वही बातें कमलेश्वर जी ने भी लिखी हैं। उनकी बातें ठीक ही लगती हैं। इसलिए आप सुदीप का परिचय तो लिखिए ही, लेकिन अब बदले हुए दृष्टिकोण से। यह भी अपनी कहानी वगैरह के साथ ही भेजने की कृपा करें। यह योजना यथाशीघ्र आरंभ हो जानी चाहिए।
मैं कहानी जब भी लिख लूँगा, आप के पास अवश्य भेजूँगा। तब तक क्षमा करेंगे।
प्रेस वाली बात अभी कुछ नहीं हुई है। देखिए।
और? पत्र दीजिएगा।
सानंद होंगे।
आपका
इब्राहीम शरीफ
मैं जुलाई, 1971 में ‘नवनीत’ की सहायक सम्पादकी और बंबई छोड़ कर दिल्ली वापस आ गया। इस बीच मैं एक बेटी का पिता बन चुका था और अब मेरा परिवार से दूर बंबई में रहना संभव नहीं था। दिल्ली आने के कुछ दिन बाद मैंने शरीफ को पत्र लिखा, जिसमें अपने बारे में बताते हुए लिखा कि जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मैं भी उसकी तरह फ्रीलांसिंग (स्वतन्त्र लेखन) करूँगा। ‘अंकन’ वाली उसकी योजना के लिए उसने मेरी ‘पुराने जूतों की जोड़ी’ कहानी माँगी थी, पर इस बीच मैं कई और कहानियाँ लिख चुका था, जो मेरी नजर में उससे बेहतर थीं। इसलिए मैंने उसे लिखा कि मैं उसकी योजना के लिए अपनी दो कहानियाँ भेजूँगा। उनमें से वह जिसे चाहे चुन ले।
मेरे पत्र के उत्तर में उसने लिखा:
54, Bazar Road
Mylapore, Madras-4
18-8-71
प्रिय भाई,
बहुत लम्बी प्रतीक्षा के बाद कल शाम को आपका पत्र मिला। जितेन्द्र ने लिखा तो था कि आप बंबई छोड़ कर दिल्ली वापस चले गये हैं। मगर चूँकि आपका दिल्ली वाला पता मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं खुद भी आपको लिख नहीं सका। अब आप मेरी ही तरह फ्रीलांसिंग करेंगे, यह जान कर बल मिला।
आपके विगत जीवन के बारे में जान कर, सच मानिए, आप से और ज्यादा निकटता अनुभव करने लग गया हूँ। बल्कि आपके प्रति इज्जत अनुभव करने लगा हूँ। मेरा जीवन भी कुछ इसी तरह का रहा है।
आपकी एक कहानी अपने पास रख लूँगा, दूसरी लौटा दूँगा। जो कहानी मैं अपने पास रख लूँगा, उसके बारे में आपका वक्तव्य (500 शब्दों का) भी चाहिए होगा। साथ में आपका चित्र भी।
मैं आपका Social Backgroundसुदीप को भेज रहा हूँ। वैसे, उन्होंने लिखा था कि सारा मैटर वे जल्दी ही भेजने वाले हैं। एक Reminder और दूँगा।
‘सारिका’ में आपकी अन्तर्कथा पढ़ी थी। बहुत पसन्द आयी।
और क्या लिख रहे हैं?
दिल्ली का जीवन कैसा है? क्या भाभी जी कहीं काम कर रही हैं?
सारी बातें लिखिएगा।
मेरी ओर से भाभी जी को नमस्कार। बच्ची को ढेरों प्यार।
पत्र देते रहिएगा।
आपका
इब्राहीम शरीफ
शरीफ के इस पत्र के उत्तर में मैंने लिखा कि मेरी पत्नी दिल्ली के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इतिहास पढ़ाती हैं। वे अपनी नौकरी तथा दिल्ली छोड़ कर कहीं और नहीं जाना चाहतीं, इसलिए मुझे अब सदा के लिए दिल्लीवासी हो कर रहना पड़ेगा, जबकि मुझे दिल्ली में कोई ढंग की नौकरी मिल नहीं रही है और स्वतन्त्र लेखन मुझे रास नहीं आ रहा है। मैं दिल्ली छोड़ कर कहीं और जाना चाहता हूँ, जहाँ मुझे कोई मनपसन्द काम मिल सके। मैंने अपनी कहानियाँ और सम्बन्धित सामग्री उसे भेज दी। कुछ समय पहले ‘अंकन’ में मेरी एक कहानी छपी थी, जिसकी प्रति मेरे पास नहीं थी। मैंने उसे लिखा कि वह मेरी उस कहानी की कतरन मुझे भेज दे। शरीफ ने मेरे इस पत्र का उत्तर काफी दिनों बाद दिया।
54, Bazar Road
Mylapore, Madras-4
2-10-71
प्रिय भाई,
आपका पत्र मिल गया था। मैं बहुत लज्जित हूँ कि आपको लिखने में देरी कर दी। यहाँ आने के बाद से जिन्दगी इतनी अस्त-व्यस्त हो गयी है कि क्या बताऊँ। फ्रीलांसिंग ने तो हालत खराब कर रखी है। जवाब देने में जो विलम्ब हो गया, उसे आप किसी भी अर्थ में उपेक्षा के रूप में मत लीजिएगा।
अब आपको दिल्ली का जीवन भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी दिल्ली मत छोडिए। कब तक इसी तरह घूमते रहेंगे?
‘धर्मयुग’ में आपका लेख देखा। पसन्द आया।
आजकल क्या लिख रहे हैं? अपने बारे में विस्तार से लिखिए।
‘अंकन’ वालों से मैं बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। मिल कर आपकी कहानी की कटिंग जरूर भेजूँगा।
हमारी योजना तो सफल होगी ही। स्थायी स्तंभ में एक-एक कहानीकार को छापना संभव न हुआ, तो एक साथ सारे कथाकारों को ‘अंकन’ के एक विशेषांक में छाप देंगे। मैं कोशिश में हूँ। अगले पत्र में इस बारे में तफसील से लिखूँगा। आपकी एक कहानी लौटा रहा हूँ। दूसरी मैंने अपने पास रख ली है। उसे तेलुगु में भी करवाने का इरादा है।
भाभी जी को मेरी तरफ से नमस्कार कहें। बच्ची को प्यार।
इस महीने के आखिर में मेरे यहाँ भी एक नये सदस्य का आगमन होगा। आपको तो लिखूँगा ही।
पत्र दीजिएगा। व्यग्र प्रतीक्षा रहेगी।
आपका
इब्राहीम शरीफ
अब याद नहीं कि शरीफ की वह कौन-सी कहानी थी, जो मुझे पसन्द नहीं आयी थी और मैंने उसकी आलोचना की थी। किस पत्रिका में वह आलोचना छपी थी, यह भी मुझे याद नहीं। मैंने उसे लिख दिया था कि मैं उस कहानी पर लिख रहा हूँ। उत्तर में उसने लिखा:
54, Bazar Road
Mylapore, Madras-4
12-10-71
प्रिय भाई,
पत्र मिला। खुशी हुई।
शायद आपको पता होगा कि आज जितेन्द्र भाटिया का जयपुर में सुधा अरोड़ा के साथ विवाह हो रहा है।
मेरी कहानी पर आपने जो भी लिखा हो, मुझे प्रसन्नता ही होगी। असल में, मैं खुद छपने के बाद उस कहानी से बेहद नाखुश हो गया था। मैंने जितेन्द्र को इस बाबत लिखा भी था। अब आगे से ऐसी रचना नहीं लिखूँगा। किसी तरह के दबाव में आ कर भी।
श्री चंद्रभूषण तिवारी ‘वाम’ निकाल रहे हैं। कल ही उनका पत्र आया है। आपको भी लिखा है।
‘कहानी’ में आपकी कहानी पढ़ी। क्या ‘कहानी’ के दीपावली अंक में आपकी कहानी आने वाली है? मेरी एक कहानी है। पढ़ कर लिखिएगा।
आपके उपन्यास की कैसी प्रगति है?
फ्रीलांसिंग वाली आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जैसा कि आपने लिखा है, क्लर्क भी, अपनी जगह, हमारी तुलना में जमा हुआ इसलिए माना जाता है कि उसे हर महीने डेढ़ सौ रुपये ही सही, बँधे हुए मिलते हैं। हम लोगों के साथ ऐसी सुविधा नहीं है। और इस तरह की सुविधा न होने में, दो तकलीफें हैं– (1) रोजमर्रे की सामान्य जरूरतों का पूरा न हो पाना (2) इन जरूरतों की पूर्ति के लिए आवश्यक रूपया कमाने के लिए अक्सर न चाहते हुए भी बहुत कुछ लिखने पर विवश हो जाना।
आप जानते हैं, आर्थिक दबाव बहुत तकलीफदेह होता है और वह समझौते करने पर मजबूर करता है। और समझौते लेखक के लिए घातक तो होते ही हैं। जैसे, आपने कोई साफ कहानी लिखी, पत्रिका वाले अपनी नीति और बिक्री के हिसाब से उसे छापने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप क्या कीजिएगा? फ्रीलांसिंग कैसे बनाये रखेंगे? नतीजा यह होता है कि या तो आप नौकरी की खोज में लग जाते हैं या कूड़ा लिखने पर विवश हो जाते हैं। ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं, कम से कम फ्रीलांसिंग की सही ताप को हल्की कर देती हैं। और इसी कारण ले-देकर लेखक समाज के साधारण अर्थ में Second Rateनागरिक बन जाता है। बात ले-दे कर यहीं आ जाती है कि सारी चीजें बदलें, खासकर राजनीतिक व्यवस्था।
आपके विचार जानना चाहूँगा।
भाभी जी को नमस्कार। बच्ची को प्यार।
आपका
इब्राहीम शरीफ
फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने शरीफ को एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें मैंने उसे बताया कि सिर्फ कहानी-उपन्यास लिख कर हिन्दी का लेखक जिन्दा नहीं रह सकता, क्योंकि रचनात्मक लेखन आप नियमित रूप से और इतना अधिक नहीं कर सकते कि उससे मासिक वेतन की तरह एक बँधी हुई रकम आपको लगातार मिलती रह सके। महीनों की मेहनत से आप एक कहानी और वर्षों की मेहनत से आप एक उपन्यास लिखते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपकी रचना छप ही जायेगी और उसका उचित पारिश्रमिक भी आपकेा मिल ही जायेगा। इसलिए मैं अपने रचनात्मक लेखन को फ्रीलांसिंग से अलग रखता हूँ। फ्रीलांसिंग के तौर पर मैं साहित्येतर विषयों पर लेख लिखता हूँ, रेडियो और टेलीविजन के लिए नाटक लिखता हूँ, अंग्रेजी और गुजराती से अनुवाद करता हूँ। कहानी किसी बड़ी पत्रिका में छप जाये और उसका उचित पारिश्रमिक मिल जाये, तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यही कारण है कि मेरी दो कहानियाँ बड़ी पत्रिकाओं में छपती हैं, तो चार छोटी पत्रिकाओं में, जो पारिश्रमिक नहीं देतीं।
मैंने उसे सलाह दी थी कि हो सके तो वह भी ऐसी ही फ्रीलांसिंग करे और अपने रचनात्मक लेखन को उससे अलग रखे। लेकिन मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। बाद के पत्र से पता चला कि पत्र तो उसने लिखा था, पर किसी कारण से वह मुझ तक पहुँचा नहीं।
मेरी पहली संतान (बड़ी बेटी प्रज्ञा) 1971 के अप्रैल महीने में पैदा हुई थी और उसी साल शरीफ अपनी पहली संतान (बडे़ बेटे राहुल) का पिता बना था। इसकी सूचना देते हुए उसने लिखा था:
54, Bazar Road
Mylapore, Madras-4
17-11-71
प्रिय भाई,
आपको मेरा पिछला पत्र मिल गया होगा। उत्तर की प्रतीक्षा थी, पता नहीं क्यों अब तक आपने उसका जवाब नहीं दिया। आशा करता हूँ, आप सपरिवार सकुशल होंगे।
आज ही मैंने आपकी टिप्पणी पढ़ी। सच मानिए, आपके सही और स्पष्ट विचारों को पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। असल में, मैं काफी कड़े शब्दों की प्रतीक्षा में था, लेकिन लगता है कि आपने फिर भी काफी उदारता दिखायी है। जैसा कि मैं आपको लिख चुका हूँ, मैं आपके विचारों से अक्षरशः सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद उस कहानी से संतुष्ट नहीं हूँ। संबंधों की ऐसी चलती हुई कहानी आगे मैं लिखने की गुस्ताखी नहीं करूँगा।
26-10-71 की सुबह हमारे घर नये मेहमान का आगमन हो गया है। पत्नी और बच्चा सकुशल हैं। बच्चे का नाम रखा है राहुल शरीफ।
आपके और क्या समाचार हैं? क्या उपन्यास वाला काम आगे बढ़ रहा है? कितना लिख लिया है? कब तक पूरा हो जायेगा? और इधर क्या लिखा है?
दिल्ली का जीवन कैसा है? पता चला है कि विश्वेश्वर, अशोक अग्रवाल वगैरह आजकल दिल्ली ही रह रहे हैं। क्या कभी उन लोगों से मुलाकात हुई है?
भाभी जी को नमस्कार कहिए। बच्ची को प्यार।
आपके पत्र की प्रतीक्षा रहेगी।
आपका
इब्राहीम शरीफ
1972 के आरंभ में शरीफ दिल्ली आया और चार महीने रहा। स्वतन्त्र लेखन में होने वाले आर्थिक कष्ट से तंग आ कर उसने दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार करने वाले मोटूरि सत्यनारायण (जिनके नाम से अब केंद्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है) की संस्था हिन्दी विकास समिति में नौकरी कर ली, जिसका एक कार्यालय मद्रास में था और दूसरा दिल्ली में। इस संस्था के द्वारा हिन्दी का पहला विश्वकोश ‘हिन्दी विश्वज्ञान संहिता’ के नाम से प्रकाशित किया जाने वाला था। वहाँ विश्वकोश के सम्पादन का काम दो व्यक्ति पहले से करते थे– एक दक्षिण भारतीय रवींद्रन और दूसरा उत्तर भारतीय गौरी शंकर। दफ्तरी काम करने वाले क्लर्क, टाइपिस्ट, चपरासी वगैरह तो थे ही।
शरीफ दिल्ली आते ही मेरे घर आ कर मुझसे मिला और बोला, ‘‘मैं चाहता हूँ कि आप हिन्दी विकास समिति द्वारा निकाले जा रहे हिन्दी विश्वकोश के सम्पादक मंडल में शामिल हो कर मेरे साथ काम करें।’’ वह मद्रास में ही मोटूरि सत्यनारायण से मेरे बारे में बात कर आया था और उनसे मेरी नियुक्ति की अनुमति लेकर आया था। मुझे नौकरी की जरूरत तो थी ही, विश्वकोश के सम्पादन जैसे महत्त्वपूर्ण काम के अनुभव का आकर्षण भी था, इसलिए मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
दिल्ली में हिन्दी विकास समिति का कार्यालय तिलक मार्ग पर उच्च न्यायालय के सामने की एक कोठी में था। उसमें एक छोटा कमरा था और एक बड़ा हॉल। कमरा प्रधान सम्पादक का था। मोटूरि सत्यनारायण विश्वकोश के प्रधान सम्पादक थे। वे जब दिल्ली में होते, उसी कमरे में बैठते और बाकी सब लोग हॉल में। उनकी अनुपस्थिति में शरीफ उस कमरे में बैठता था। इस प्रकार वह हम सबका बॉस था, लेकिन उसमें अफसरी अकड़ नहीं थी। उसका व्यवहार सभी के साथ दोस्ताना था। लंच के समय वह और मैं उच्च न्यायालय परिसर के एक ढाबे पर खाना खाने जाते और सर्दियों की धूप में कुछ देर सड़क पर टहलते हुए गपशप करते। शरीफ बहुत हँसमुख था और बहुत अच्छा किस्सागो। दिल्ली में उसके दो पुराने मित्र थे– उत्तर भारतीय सुधीर चौहान और दक्षिण भारतीय जे.एल. रेड्डी। वे दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी प्राध्यापक थे। शरीफ के कारण मेरी भी उनसे मित्रता हो गयी। बाद में जब मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गया, तो उन दोनों से मेरी मित्रता और प्रगाढ़ हुई, जो आज तक कायम है, जबकि हम तीनों प्राध्यापकी से मुक्त हो चुके हैं।
शरीफ मेरे घर अक्सर आया करता था। मेरे परिवार में सब लोगों से वह खूब घुलमिल गया था। हँसी-मजाक में एक दिन हम लोगों ने फिल्मी तर्ज पर तय किया कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जायेंगे, हम उनकी शादी करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। तभी से शरीफ मेरी बेटी प्रज्ञा को बहूरानी कहने लगा और मैं उसके बेटे राहुल को दामाद जी। यह सम्बन्ध बाद में हमारे पत्राचार में भी व्यक्त होता रहा।

चार महीने बाद शरीफ वापस मद्रास चला गया, लेकिन वहाँ जा कर भी वह हिन्दी विकास समिति का काम करता रहा। उसका वेतन दिल्ली से उसे भेजा जाता था। मद्रास जाते समय वह अपनी कुर्सी और जिम्मेदारी मुझे सौंप गया। अर्थात्, जब मोटूरि सत्यनारायण और इब्राहीम शरीफ दिल्ली में नहीं होंगे, विश्वकोश के प्रधान सम्पादक के कमरे में बैठ कर दफ्तर का सारा कामकाज मुझे देखना होगा। लेकिन यह बात वहाँ मुझसे पहले से काम करने वाले रवींद्रन और गौरीशंकर को अच्छी नहीं लगी। वहाँ उनकी नियुक्ति मुझसे पहले हुई थी, इसलिए वे वरीयता क्रम में स्वयं को मुझ से ऊपर समझते थे। मेरे आदेशों का पालन करने में उन्हें अपनी हेठी लगती थी, इसलिए वे मेरे द्वारा बताये गये कामों को टाल देते थे या उनमें जान-बूझकर ढिलाई बरतते थे। इससे काम की गति तो धीमी होती ही थी, दफ्तर में एक तरह का तनाव भी पैदा होता था। शरीफ मद्रास से पत्र लिख कर पूछता था कि दफ्तर का कामकाज कैसा चल रहा है। उसका कहना था कि मोटूरि सत्यनारायण हर हफ्ते काम की प्रगति की विस्तृत रपट चाहते हैं। काम उसकी, और मेरी भी, अपेक्षा के मुताबिक तेजी से नहीं हो रहा था। मगर मैं अपने साथ काम करने वालों की शिकायत नहीं करना चाहता था, इसलिए शरीफ के पत्रों के उत्तर देना या तो गोल कर जाता, या बहुत संक्षेप में उत्तर देता। उसके दोस्त सुधीर चौहान और जे.एल. रेड्डी दफ्तर की दशा जानते थे, पर मैंने उनसे भी कह रखा था कि इस बाबत शरीफ को लिख कर उसे परेशान न करें।
उधर शरीफ इसी बात से चिंतित और परेशान रहता था। इस बीच वह मुझ से बहुत निकटता और आत्मीयता अनुभव करने लगा था, इसलिए उसके पत्रों में ‘‘प्रिय भाई’’ वाला औपचारिक संबोधन बदल कर ‘‘प्रिय रमेश’’ हो गया था। पत्र के नीचे भी अब वह ‘‘आपका इब्राहीम शरीफ’’ लिखने की जगह ‘‘तुम्हारा शरीफ’’ लिखता था। उन्हीं दिनों का उसका एक पत्र है:
54, Bazar Road
Mylapore, Madras-4
26-6-72
प्रिय रमेश,
मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं आ रही है जिसके अन्तर्गत मैंने तुम्हारे प्रति इस हद तक गुस्ताखी की हो कि तुम मेरे खत का जवाब देना तक गवारा न कर सको। अगर मुझसे ऐसी कोई भूल हो गयी हो तो मुझे माफ कर दो, मेरे भाई!
तुम बखूबी सोच सकते हो कि चार महीने लगातार तुम्हारी आत्मीयता पा कर मैं इतनी दूर आ जाऊँ और तुम मेरे पत्र का जवाब तक न दो, तो मुझे किस हद तक तकलीफ हो सकती है। मैं यह तो बिलकुल नहीं मान सकता कि तुम्हें इतनी भी फुर्सत न मिलती हो कि चार अक्षर तुम मुझे लिख सको। इसलिए मैं यह सोचने पर विवश हूँ कि मुझसे कोई भूल हो गयी है, जिसकी वजह से तुम भरे बैठे हो। तो मेरे भाई, गाली-गलौज ही क्यों नहीं दे लेते, जिससे पता तो चले कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। सिर्फ दफ्तरी पत्र पाने ही के लिए तो मैंने तुमसे दोस्ती नहीं की थी न?
मैंने अपने 16-6-72 वाले विस्तृत पत्र में तुम्हें बहुत सारी बातें लिखी थीं। तुमने उन बातों में कोई जान नहीं देखी कि चुप्पी साध गये? आखिर तुम्हें हो क्या गया है, रमेश? क्या तुम वही रमेश हो, प्यारे, भोले और आत्मीय, जिसे मैंने चार महीने जाना और चाहा था?
अगर तुम इस पत्र का भी जवाब नहीं दोगे, तो याद रखो, मैं जिन्दगी में किसी पर भी कोई विश्वास नहीं करूँगा। उस गधे चौहान से भी कहो कि उसने भी मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया है।
भाभी जी के क्या हाल हैं? उन्हें मेरी नमस्ते कहो और बहूरानी को ढेरों प्यार।
तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में,
तुम्हारा
शरीफ
हिन्दी विकास समिति मोटूरि सत्यनारायण द्वारा स्थापित एक गैर-सरकारी संस्था थी, जो सरकारी सहायता से चलती थी। वे दक्षिण में हिन्दी का प्रचार करने वाले एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में विख्यात थे और हिन्दी में पहला विश्वकोश निकालने की उनकी योजना बहुत प्रभावशाली थी, अतः अपनी संस्था के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वे संस्था के सर्वेसर्वा थे और तानाशाह की तरह उसे चलाते थे। जब जिसे चाहा, रख लिया; जब जिसे चाहा, हटा दिया। लेकिन यह काम वे सीधे नहीं करते थे, शरीफ से कराते थे और शरीफ न चाहते हुए भी उनके आदेशों का पालन करने को विवश होता था।
शरीफ उस नौकरी में खुश नहीं था, लेकिन उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। वह कालीकट के जिस कॉलेज में हिन्दी प्राध्यापक रह चुका था, वहाँ के हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. मलिक चाहते थे कि वह पुनः कॉलेज में पढ़ाने आ जाये। लेकिन शरीफ की न जाने क्या मजबूरी थी कि वह वहाँ नहीं जाना चाहता था।
कमलेश्वर ने शरीफ को ही नहीं, मुझे भी यह आश्वासन दे रखा था कि वे हम दोनों को टाइम्स ऑफ इंडिया में, यानी उस प्रकाशन समूह की ‘धर्मयुग’, ‘सारिका’, ‘दिनमान’ या ‘पराग’ नामक पत्रिकाओं में से किसी के सम्पादकीय विभाग में नौकरी दिला देंगे। लेकिन उनका कोई आश्वासन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था।
शरीफ और मैं अपने लिए कोई ढंग का ठौर-ठिकाना ढूँढ़ रहे थे, लेकिन विडंबना यह थी कि अन्य लोग हमें इतना शक्तिशाली समझते थे कि हम जिसे चाहें, हिन्दी विकास समिति में नौकरी पर रख या रखवा सकते हैं। मेरे और शरीफ के साझे मित्र कहानीकार सतीश जमाली को नौकरी की जरूरत थी और वह चाहता था कि हम उसे समिति में नौकरी दिला दें। मैंने शरीफ से सतीश के बारे में बात की, तो उसने किन्हीं डॉ. सुब्रह्मण्यम् के बारे में बताया कि उन्हें नौकरी की ज्यादा जरूरत है और शरीफ उन्हें समिति के मद्रास कार्यालय में रखवाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए फिलहाल सतीश के लिए कुछ नहीं कर सकता।
इन सारे संदर्भों से युक्त शरीफ का एक पत्र इस प्रकार था:
54, Bazar Road
Mylapore, Madras-4
28-6-72
मेरे रमेश,
आखिर तुम्हारा एक खत मिला, संक्षिप्त-सा। पढ़ कर तसल्ली तो हुई मगर मजा नहीं आया।
यार, चौहान और तुम्हारे नाम लिखे हुए मेरे पत्र जा कहाँ रहे हैं? और लोगों को मेरे पत्र मिल रहे हैं और तुम दोनों सालो मेरे पत्र न मिलने का बहाना कर चुप्पी साधे बैठे हो। मैंने तुम दोनों के नाम और दो पत्र लिखे हैं।
क्या कमलेश्वर जी दिल्ली आये थे? क्या बातें हुईं? वह टाइम्स वाली बात उन्होंने कुछ नहीं लिखी है। पता नहीं क्या हुआ?
डॉ. मलिक कालीकट बहुत जोर देकर बुला रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक कुछ तय नहीं कर पाया हूँ। डॉ. सुब्रह्मण्यम, जिसके बारे में मैंने बताया था कि बेचारा यहाँ सभा की नौकरी से हटा दिया गया था, उसके लिए मैंने हिन्दी विकास समिति में यहाँ के लिए इंतजाम कर लिया है। जुलाई की पहली से संभवतः वह लग जाये। अब यार, सतीश जमाली की चिन्ता है। उसके लिए कुछ करें, तभी बात बने। उसकी नौकरी छूटने वाली है और बेकारी में बेचारा कैसे घर चला पायेगा? तुम भी कुछ सोचो उस भाई के लिए।
यहाँ से निकलने वाली पत्रिका का क्या सोचा है तुम लोगों ने? कमलेश्वर जी के साथ हुई बातचीत का ब्योरेवार परिचय मुझे दो।
मेरे वेतन में से 100 रुपये इस महीने मत काटो। मुझे घर जाना है, भाई के बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं। मुझे रुपयों की जरूरत होगी।
और?
मेरी बहूरानी के क्या हाल हैं? उसे उसके ‘वो’ बहुत याद करते रहते हैं। उसकी सास को तो वह बहुत पसन्द आयी है। कहती है, बहुत Sweet है।
भाभी जी को सादर नमस्कार। मेरी बीवी की ओर से तुम दोनों को प्रणाम।
उस चौहान गधे के क्या हाल हैं? लिखो।
तुम्हारा
शरीफ
जिस संस्था में तानाशाही और अस्थायित्व हो, उसमें काम करने वाले लोग असुरक्षा की मानसिकता में जीते हुए एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त हो जाते हैं। हिन्दी विकास समिति के दिल्ली कार्यालय में मेरे साथ काम करने वाले रवींद्रन और गौरीशंकर मेरे प्रति ऐसे ही ईर्ष्या-द्वेष से ग्रस्त थे। वे मेरे विरुद्ध शरीफ को भड़काने वाले पत्र तो लिखते ही थे, विश्वकोश से सम्बन्धित काम भी मुस्तैदी से नहीं करते थे। उधर मोटूरि सत्यनारायण का शरीफ पर और शरीफ का मुझ पर निरंतर यह दबाव रहता था कि विश्वकोश के पहले खण्ड का प्रकाशन जल्दी से जल्दी हो जाये। शायद इसी पर सरकारी अनुदान मिलना निर्भर करता था। अन्ततः मुझे एक पत्र में दफ्तर का सारा हाल शरीफ को लिखना पड़ा। मेरे पत्र के उत्तर में शरीफ के दो पत्र आये, एक दफ्तरी और दूसरा निजी। निजी पत्र इस प्रकार था:
54, Bazar Road
Mylapore, Madras-4
13-7-72
प्रिय रमेश,
तुम्हारा खत मिला।
आज सुबह ही मैंने तुम्हारे नाम दफ्तर के पते पर एक पत्र भेजा है, जिसमें मैंने तुम तीनों को संबोधित किया है। मैंने अब तक का सारा दफ्तर का पत्र-व्यवहार सत्यनारायण जी को दिखाया है और जो कुछ मैंने तुम लोगों को लिखा है, वह सब उन्हीं के आदेशानुसार लिखा है। तुम जानते हो, मैं भी तुम लोगों की तरह ही नौकर हूँ और मुझे जो आदेश दिया जाता है, वह करना मेरा कर्तव्य हो जाता है।
गौरी के बारे में तुमने जो बातें लिखी थीं, वे सारी सत्यनारायण जी पहले ही से जानते हैं। और उन्होंने मुझे बताया भी था। इस सबके बावजूद, हो सकता है, गौरी या रवींद्रन या तुम खुद भी मुझे गलत समझ सकते हो। लेकिन मेरे भाई, शायद तुम अपने चार महीनों के अनुभव के आधार पर इतना तो जान गये होगे कि मैं न किसी की बुराई चाहता हूँ, न किसी पर कोई अधिकार चलाना चाहता हूँ। गौरी खुद ये सारी बातें जानता है। मगर वह इतना रूखा इंसान है कि व्यक्तिगत संबंधों को कोई तरजीह नहीं देता है। खैर, मेरी असलियत मेरे साथ है, तुम लोग जो भी समझो।
मैं खुद इस नौकरी में बहुत दिन नहीं रहूँगा। ताकि तुम लोग मुझे और ज्यादा गलत समझने का मौका न पा सको। खैर, ये तो दफ्तर की बेहूदा बातें हैं।
कमलेश्वर जी के पत्र आये। ‘समांतर’ संग्रह के लिए उन्होंने मेरी ‘दिग्भ्रमित’ कहानी चाही है। उसकी कटिंग मेरे पास नहीं है। यहाँ मिलने की भी संभावना नहीं है। तुम्हारे पास ‘धर्मयुग’ के पुराने अंक हों, तो (4 अक्टृबर, 1970 के अंक से) कटिंग तत्काल कमलेश्वर जी के पास भेजो। श्रवण कुमार बता रहे थे कि मेरी उस कहानी की कटिंग उनके पास भी है। उन्हें भी पूछो। उनके पास हो, तो लेकर बंबई भेज दो।
और?
सतीश के बारे में अभी कोई व्यवस्था करने की स्थिति नहीं है। पहली जिल्द निकलने के बाद ही वह संभव हो पायेगा। इसलिए इस नवंबर-दिसंबर के पहले नहीं हो पायेगा। मैंने कमलेश्वर जी को भी यही बातें सूचित की हैं। तुम भी लिख दो।
और क्या हो रहा है?
भाभी जी को प्रणाम। बच्ची को प्यार। पत्र दो। कहानी बंबई भिजवाओ।
तुम्हारा
शरीफ
‘प्रिय भाई’, ‘प्रिय रमेश’, ‘मेरे रमेश’ जैसे संबोधनों वाले पत्र लिखने वाले शरीफ ने एक बार मुझे ‘अप्रिय रमेश’ लिखकर भी संबोधित किया था:
54, Bazar Road
Mylapore, Madras-4
26-8-72
अप्रिय रमेश,
लगता है, मुझे भाभी जी से यह जानना पड़ेगा कि तुम अपने-आपको क्या समझते हो! यार, पत्र क्यों नहीं लिखते? दफ्तर पर पत्र लिखा, जवाब नहीं। घर के पते पर लिखा, वही मौन। लगता है, निर्दयी होते जा रहे हो। खासकर मेरे साथ। खासकर तुम्हारी प्यारी बिटिया के ससुर के साथ।
खुश हो जाओ कि अगले महीने की दूसरी तारीख तक बंदा दिल्ली पहुँच रहा है। सत्यनारायण जी भी चाहते हैं। एक तार भिजवाया था सत्यनारायण जी ने तुम्हारे नाम–मेरे द्वारा (यानी मेरा नाम रख कर) घबराने की कोई बात नहीं। संक्षेप में लिखो कि कितना काम हुआ है। उन्हें इन बातों को बार-बार जानने की लत है।
यह पत्र, ध्यान रखो कि एकदम व्यक्तिगत है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। बाहर न जाये।
भाभी जी को प्रणाम।
बिटिया को प्यार।
तत्क्षण लिखो।
तुम्हारा
शरीफ
सितंबर, 1972 में शरीफ दिल्ली आ गया, तो मुझे दफ्तर की उस जिम्मेदारी से मुक्ति मिली, जिसे सँभालने के बदले में मेरा वेतन तो एक पैसा भी नहीं बढ़ा था, पर सिरदर्दी बहुत बढ़ गयी थी। शरीफ अपने कमरे में बैठने लगा और मैं वापस हॉल में अपनी पहली वाली जगह। मुझे तो इससे तनावमुक्त हो जाने की खुशी हुई, लेकिन रवींद्रन और गौरीशंकर को इस बात की खुशी हुई कि मैं अब उनका सीनियर नहीं रहा, बल्कि नियुक्ति के तिथि-क्रम के अनुसार पुनः उन दोनों से जूनियर हो गया हूँ।
मुझे इसकी परवाह नहीं थी, बल्कि खुशी थी कि मेरा बहुत-सा समय बच गया, जो शरीफ की जगह बैठने से विश्वकोश के लेखकों को टेलीफोन करके काम जल्दी करने के लिए कहने में, टाइपिस्ट को काम देने, उसके काम को जाँचने और उसे ठीक से काम करने की ताईद करने में तथा कारण-अकारण मिलने आने वालों के साथ बातचीत करने में चला जाता था। वापस अपनी जगह आ कर मैंने सम्पादन का काम तेजी से करना शुरू किया। देखा-देखी रवींद्रन और गौरीशंकर भी मुस्तैदी से काम करने लगे।
उन्हीं दिनों कानपुर में ‘समांतर’ का दूसरा सम्मेलन हुआ, जिसमें शरीफ और मैं दिल्ली से साथ-साथ गये। सम्मेलन 15, 16, 17 अक्टूबर को होना था, लेकिन कमलेश्वर ने मुझे, शरीफ, जितेन्द्र और मधुकर सिंह को एक दिन पहले कानपुर पहुँच जाने के लिए कहा था, ताकि ‘‘समांतर के कोर ग्रुप’’ के लोग (अर्थात् कमलेश्वर, मैं, शरीफ, जितेन्द्र, कामतानाथ और मधुकर सिंह) पहले मिल कर तय कर लें कि सम्मेलन में क्या-क्या और किस तरह किया जाना है।
मैं और शरीफ 13 अक्टूबर को रात की गाड़ी से कानपुर गये। रास्ते में समांतर को लेकर शरीफ से मेरी लम्बी बातचीत हुई। हम दोनों के विचार से कमलेश्वर ने हमारे आन्दोलन को चालाकी से हथियाकर अपना नेतृत्व उस पर थोप दिया था। गलती हम लोगों की भी थी कि हमने अपना आन्दोलन स्वयं चलाने के बजाय उसकी बागडोर उनके हाथ सौंप दी। होना यह चाहिए था कि हम अपना आन्दोलन अपने ढंग से चलाते, उसके लिए एक नया मंच बनाते और उसके जरिये कहानी के रूप तथा वस्तु-तत्त्व में आ रहे नये बदलाव को उसके मूल्य और महत्त्व के साथ सामने लाते। उस समय हिन्दी साहित्य में पुराने प्रगतिशील आन्दोलन का जो नया उभार वाम-जनवादी लेखन के रूप में सामने आ रहा था, उससे जुड़ कर हमें एक नया कहानी आन्दोलन शुरू करना चाहिए था और ‘पहल’, ‘वाम’, ‘उत्तरार्द्ध’ आदि पत्रिकाओं जैसी कोई नयी पत्रिका निकाल कर उस समय लिखी जा रही वाम-जनवादी कहानी को एक नये साहित्यिक आन्दोलन का रूप देना चाहिए था। लेकिन हमने तत्कालीन सत्ता और व्यवस्था के समर्थक एक पुराने लेखक को अपना नेता तथा एक पूँजीवादी संस्थान से निकलने वाली व्यावसायिक पत्रिका को अपना मंच मान लिया था। समांतर आन्दोलन में शामिल ज्यादातर कहानीकार अराजनीतिक किस्म के लेखक थे और कमलेश्वर ‘नयी कहानी’ आन्दोलन के समाप्त हो जाने पर साहित्य में अपनी साख और धाक फिर से जमाने की फिराक में थे। फिर, एक तरफ कमलेश्वर को कहानी की एक पत्रिका चलाने के लिए लगातार अच्छी कहानियों की जरूरत थी, जो नये कहानीकार ही पूरी कर सकते थे, तो दूसरी तरफ नये कहानीकारों को ‘सारिका’ जैसी लोकप्रिय पत्रिका में निरंतर प्रकाशित होने और उसके सम्पादक की निकटता का लाभ उठा कर साहित्य में अपने पैर जमाने का अवसर मिल रहा था। इस प्रकार पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर समांतर कहानी का आन्दोलन चल रहा था।
उस समय हिन्दी साहित्य में वाम-जनवादी लेखन का जो नया उभार आया हुआ था, उससे जुड़े लेखक तथा साहित्यिक पत्रिकाओं के सम्पादक मार्क्सवादी थे और वाम दलों के सदस्य अथवा समर्थक थे। हम साहित्य की उस नयी प्रवृत्ति से जुड़ कर अपना कहानी आन्दोलन चलाते, तो हमारे आन्दोलन की दशा और दिशा कुछ और ही होती। लेकिन समांतर आन्दोलन उस नयी प्रवृत्ति के विरोधी उन लेखकों का एक गुट बन कर रह गया, जो मार्क्सवाद तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी थे।
मैं शरीफ से दोस्ती होने से पहले से ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक था (यद्यपि मैं उसका सदस्य कभी नहीं रहा) और मेरी गिनती वाम-जनवादी लेखकों में होने लगी थी। कमलेश्वर चाहते थे कि समांतरी लेखक वाम राजनीति और विचारधारा से कोई सम्बन्ध न रखें। ज्यादातर समांतरी लेखक उनसे सहमत थे। उनकी दलगत संबद्धताएँ जो भी रही हों, या न रही हों, उन सब में एक चीज समान थी- सी. पी. एम. का विरोधी होना। कामता नाथ सी. पी. एम. वालों की तीखी आलोचना किया करता था, मधुकर सिंह सी. पी. एम. के ई. एम. एस. नंबूदिरिपाद जैसे नेताओं तक को गालियाँ दिया करता था, जितेन्द्र भाटिया राजनीति से अलग और ऊपर रहने की बातें किया करता था और शरीफ सभी प्रकार की राजनीति से नफरत-सी किया करता था। (यह नफरत उसकी ‘दिग्भ्रमित’ जैसी कहानियों में भी दिखायी देती थी।) कमलेश्वर सी. पी. एम. की आलोचना करने और उसके नेताओं को गाली देने के बजाय उनका मजाक उड़ाने के जरिये अपना विरोध प्रकट करते थे। मसलन, ‘वाम’ के सम्पादक चंद्रभूषण तिवारी को ‘चंभूति’ कह कर वे ठहाके लगाया करते थे।
मैंने और शरीफ ने तय किया कि हम कानपुर में होने जा रहे समांतर के दूसरे सम्मेलन में अपने आन्दोलन की राजनीतिक पक्षधरता और प्रतिबद्धता स्पष्ट करने पर जोर देंगे।
हम 14 अक्टूबर को सुबह के ढाई बजे कानपुर पहुँचे। हमें कामता नाथ के घर पहुँचना था, लेकिन इतने सवेरे उसके घर पर दस्तक देना उचित न समझ हमने स्टेशन पर अपना सामान रखा, एक रिक्शा किया और उस पर शहर में घूमते रहे। रमजान का महीना था, इसलिए मुसलमान लोग दिन भर के उपवास के लिए खा-पी कर तैयार होते दिखे। रिक्शे वाला भी मुसलमान था, पर उसने बताया कि वह रोजे नहीं रखता, क्योंकि रोजा रख कर रिक्शा नहीं चला सकता। एक जगह रुक कर हमने चाय पी, उसे भी पिलायी और वह हमारे कहने पर हमें कानपुर के मुस्लिम इलाकों में ले गया। दो कब्रिस्तानों के बीच की एकदम अँधेरी सड़क से भी हम गुजरे। सुबह की शबनमी ठंड में पाँच बजे तक घूम कर हम स्टेशन लौटे। तभी कलकत्ता से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस से जितेन्द्र उतरा। वह कलकत्ता से आया था। उसके साथ हम कामता नाथ के घर गये। कमलेश्वर के बंबई से और मधुकर सिंह के आरा से आ जाने पर सम्मेलन की रूपरेखा पर विचार हुआ।
उस समय कानपुर में सी. पी. एम. का बड़ा सशक्त मजदूर संगठन था। कॉमरेड राम आसरे और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में रहीं कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी सुभाषिनी सहगल (जो बाद में मुजफ्फर अली से शादी करके सुभाषिनी अली और सी. पी. एम. की बड़ी नेता बनी) वहाँ के दो बड़े लोकप्रिय मजदूर नेता थे। सुभाषिनी से कुछ दिन पहले दिल्ली में मेरी भेंट हुई थी। मैंने उसे कानपुर में होने वाले समांतर सम्मेलन के बारे में बताया था। उसे यह बात याद रही और वह सम्मेलन में मुझ से मिलने आयी। मेरे कहने पर एक गोष्ठी में उपस्थित रही और बोली भी। मैंने शरीफ और जितेन्द्र को अलग ले जा कर उस से मिलवाया, तो उसने हम तीनों से बात करने के लिए हमें सम्मेलन-स्थल के निकट ही रहने वाले अपने एक कॉमरेड के घर ले जा कर चाय पिलायी और यह जान कर कि शरीफ मद्रास से एक उर्दू अखबार निकालने की सोच रहा है, उसने शरीफ को मद्रास के अपने कुछ साथियों के पते दिये, जो अखबार निकालने में शरीफ की मदद कर सकते थे।

कमलेश्वर को समांतर सम्मेलन में सुभाषिनी का आना, हम तीनों से उसका बातचीत करना और हमारा उसके साथ चाय पीने जाना अच्छा नहीं लगा। रात को कामतानाथ के घर पर हुई दारू-पार्टी में कमलेश्वर ने मुझ से कहा, ‘‘रमेश, सी. पी. एम. वाले तुम्हें ओन करने लगे हैं, यह गलत बात है।’’ उन्हें इस पर भी ऐतराज था कि मैंने शरीफ और जितेन्द्र को सुभाषिनी से क्यों मिलवाया और क्यों मैं उन दोनों को लेकर उसके साथ चाय पीने गया। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने पूछा, ‘‘क्या समांतर के लेखकों को यह आजादी नहीं कि वे अपनी मर्जी से अपने मित्रों के साथ कहीं चाय पीने भी जा सकें?’’
गंभीर बातों को हँसी-मजाक में उड़ा देने की कूट-कला में माहिर कमलेश्वर ने इस विषय पर आगे बात नहीं होने दी और शराब की चुस्कियों के साथ उनकी चुटकुलेबाजी शुरू हो गयी। मुझे यह बात आश्चर्यजनक लगी कि शरीफ और जितेन्द्र ने भी वह बात आगे नहीं बढ़ायी।
मैंने कानपुर में ही फैसला कर लिया था कि मैं समांतर में नहीं रहूँगा। लेकिन शरीफ और जितेन्द्र अपना भविष्य शायद समांतर में बने रहने में ही देख रहे थे। अतः दोनों मुझे समझाते रहे कि मैं समांतर छोड़ने की गलती न करूँ।
उन दिनों बड़ी (व्यावसायिक) पत्रिकाओं के विरुद्ध लघु (साहित्यिक) पत्रिकाओं का आन्दोलन जोर-शोर से चल रहा था और कई लेखकों ने, जो अभी तक बड़ी पत्रिकाओं में धड़ल्ले से छपते आ रहे थे, उनमें न लिखने का फैसला किया था। मैं उन दिनों ‘धर्मयुग’, ‘सारिका’, ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’ आदि बड़ी पत्रिकाओं में खूब लिखता था। ‘धर्मयुग’ और ‘सारिका’ टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन से निकलने वाली बड़ी पत्रिकाएँ थीं, जिनमें मेरी कहानियाँ खूब छपती थीं। टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस बंबई में बोरीबंदर के पास था। बोरीबंदर के नाम से जोड़ कर रवींद्र कालिया ने मुझे कहीं ‘‘बोरीबंदर का लाडला कथाकार’’ कहा था और उसका यह जुमला खूब चला था। फिर भी मैंने लघु पत्रिका आन्दोलन में शामिल हो कर बड़ी पत्रिकाओं में न लिखने का फैसला किया। ‘सारिका’ बड़ी पत्रिका थी और वह समांतर आन्दोलन की पत्रिका भी थी। इसलिए ‘सारिका’ से नाता तोड़ने का अर्थ अपने-आप ही ‘समांतर’ से नाता तोड़ना भी हो गया।
शरीफ को मेरा यह निर्णय अच्छा नहीं लगा। उसने और समांतर से जुड़े अन्य लेखकों ने भी ‘सारिका’ और ‘समांतर’ से जुड़े रहने में ही अपनी भलाई देखी।
कानपुर से लौटने के कुछ दिन बाद शरीफ पुनः मद्रास चला गया। हिन्दी विकास समिति में विश्वकोश का पहला खण्ड छपने चला गया था और अगले खण्ड के सम्पादन का काम शुरू होने में अभी देर थी, इसलिए मोटूरि सत्यनारायण ने शरीफ से कहा कि कुछ समय के लिए दिल्ली दफ्तर से किसी एक व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया जाये। जब जरूरत होगी, उसे फिर से रख लेंगे। तदनुसार शरीफ ने मुझे लिखा:
54, Bazar Road
Mylapore, Madras-4
28-10-72
प्रिय रमेश,
तुम्हारा लंबा पत्र मिल गया था। मुझे खुद लिखना चाहिए था। मगर लिख नहीं सका। इस बार तुमसे दूर होकर मुझे कुछ अतिरिक्त बेचैनी हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह कि जिस नौकरी पर मैंने अपनी तरफ से तुम्हें लगाया था, उसकी रक्षा मैं खुद करने की हालत में फिलहाल नहीं रह गया हूँ। तुम जानते ही हो कि अब दफ्तर में काम कम है और इसलिए किसी एक को दो-एक महीने के लिए हटाना जरूरी है। मैं चाहता, तो गौरी को भी हटा सकता था, लेकिन तुम्हारे सामने क्या छिपाना कि मैंने तुम्हें ही हटाने की बात सत्यनारायण जी से कही है। वह इसलिए कि तुम नौकरी के बगैर भी एक-दो महीने चला सकते हो, मगर वह नहीं। यह बात मैं तुम्हें साफ लिख रहा हूँ, ताकि तुम कभी भी मुझे गलत न समझो।
मैं वादा करता हूँ कि जनवरी से फिर से तुम्हें वहाँ रखवाऊँगा। श्री रवींद्रन के लिए मैंने कालीकट वाली व्यवस्था कर दी है। उन्हें निश्चित रूप से छात्रवृत्ति मिल जायेगी दिसंबर में। वे चले जायेंगे और मैं तुम्हें फिर से रखवा लूँगा। और इस बार कुछ महीनों के लिए नहीं, कई सालों के लिए, अगर तुम चाहोगे, तो। सत्यनारायण जी भी तुम्हें बहुत चाहते हैं। लेकिन अभी वे भी विवश हैं। तुम नवंबर की पहली तारीख से दफ्तर मत जाओ। मैं तुम्हें Officially न लिख कर व्यक्तिगत रूप से लिख रहा हूँ, एक भाई के नाते। तुम सत्यनारायण जी से मेरे पत्र का जिक्र करो और उन्हें बता दो कि पहली नवंबर से तुम काम पर नहीं आओगे, अगली सूचना तक।
मेरे भाई, यह पत्र लिखते हुए मैं क्या कुछ अनुभव कर रहा हूँ, तुम्हें बता नहीं सकता। खैर, तुम मुझे गलत नहीं समझोगे, इस आशा के साथ।
मैंने कमलेश्वर जी को उर्दू पत्रिका वाली योजना भेज दी है। देखें, क्या होता है। तुम अपनी बातें लिखो।
भाभी जी को प्रणाम। बिटिया को बहुत-बहुत प्यार।
पत्र तत्काल दो।
तुम्हारा
शरीफ
हिन्दी विकास समिति की नौकरी खत्म होने का मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि एक बेमतलब तनाव से मुक्त होने की खुशी ही हुई। मैंने मोटूरि सत्यनारायण को अपना त्याग-पत्र तो भेजा ही, शरीफ को भी लिख दिया कि वह मेरी चिन्ता न करे, मुझे इस नौकरी में वापस कभी नहीं आना है और इस प्रसंग का हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ना है।
मैं फ्रीलांसिंग और अस्थायी नौकरियों के अपने अनुभव से अच्छी तरह समझ चुका था कि हिन्दी में स्वतन्त्र लेखन के सहारे जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने प्राध्यापक बनने के वास्ते पी-एच. डी. के लिए शोध करना शुरू कर दिया था। शरीफ मुझसे पहले ही पी-एच.डी. कर चुका था। उसने आगरा विश्वविद्यालय से ‘दक्खिनी हिन्दी के लोकगीत’ विषय पर पी-एच.डी. की थी। उससे मैंने कई बार कहा कि वह कोई स्थायी नौकरी खोजे और आजीविका की ओर से निश्चिंत हो कर अपना साहित्य-सृजन करे। यदि डॉ. मलिक अपने कॉलेज में प्राध्यापक बनाने के लिए उसे कालीकट बुला रहे हैं, तो उसे वहाँ अवश्य चले जाना चाहिए। लेकिन शरीफ की न जाने वह कौन-सी जिद या मजबूरी थी कि वह हिन्दी विकास समिति की नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं था और उसमें रहकर खुश भी नहीं था। वह मद्रास में ही रह कर कोई ऐसा काम करना चाहता था, जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। पहले उसने वहाँ प्रेस लगाने की योजना बनायी। फिर हिन्दी की साहित्यिक पत्रिका निकालने की योजना बनायी। फिर उर्दू का अखबार और उसकी जगह फिर उर्दू में पत्रिका निकालने की योजना बनायी। मगर कोई योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कोई काम शुरू करने के लिए जरूरी पैसा उसके पास नहीं था।
कमलेश्वर तब तक हिन्दी फिल्मों के पटकथा लेखक बन चुके थे। उन्होंने शरीफ को जिस तरह टाइम्स ऑफ इंडिया की किसी पत्रिका में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था, या जैसे उसके द्वारा निकाले जाने वाले उर्दू अखबार के लिए सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया था, वैसे ही फिल्मों में काम दिलाने का आश्वासन भी दिया। लेकिन वे सब हवाई बातें थीं, जिनके कारण अन्ततः कमलेश्वर और समांतर आन्दोलन से भी उसका मोह-भंग हुआ। फिर भी न जाने क्यों, वह मेरी तरह उससे अलग कभी नहीं हुआ।
मैंने उससे यह भी कहा था कि वह वाम-जनवादी साहित्य और लघु पत्रिकाओं के आन्दोलन से अपना सम्बन्ध स्पष्ट कर ले। किन्तु वह सोचता था कि बड़ी पत्रिकाओं में लिखना छोड़ कर पारिश्रमिक न देने वाली लघु पत्रिकाओं में लिखने का फैसला करके वह जिन्दा नहीं रह सकेगा। समांतर आन्दोलन को भी वह शायद इसीलिए छोड़ना नहीं चाहता था।
इधर वाम-जनवादी आन्दोलन में एक नया उभार आया देख प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े लोगों ने उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 1973 में ‘‘सभी रंगतों के प्रगतिशील’’ लेखकों का एक बड़ा सम्मेलन बाँदा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित किया। मुझे भी उसमें बुलाया गया था। मैंने शरीफ को लिखा कि वह भी उस सम्मेलन में शामिल हो। मगर वह समांतर से इतना निराश हो चुका था कि बाँदा सम्मेलन को भी समांतर सम्मेलन जैसी ही कोई चीज समझ रहा था, जिसमें रात को शराब की चुस्कियों के साथ चुटकुलेबाजी होती थी।
मैंने उसे एक विस्तृत पत्र लिख कर उसे समांतर सम्मेलन और बाँदा के प्रगतिशील साहित्यकार सम्मेलन का फर्क समझाते हुए बाँदा चलने के लिए कहा, तो उत्तर में उसने लिखा:
54, Bazar Road
Mylapore, Madras-4
9-2-73
प्रिय रमेश,
तुम्हारा विस्तृत पत्र कल शाम को मिला।
बाँदा वाले सम्मेलन में मैं नहीं जाऊँगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं शराब पीने के लिए और चुटकुले सुनने-सुनाने के लिए उतनी दूर जाऊँ। जितेन्द्र ने भी मुझसे आग्रह किया था कि मैं चलूँ। कमलेश्वर जी ने भी लिखा था। मैंने मना कर दिया है। ‘समांतर’ के अन्तर्गत हम लोग दो बार मिले हैं। कोई काम हुआ है? कोई योजना पूरी हुई है? कोई महान कहानी-उपन्यास-नाटक लिखा गया है? या कम से कम सारे ‘समांतरी’ एक तरह सोच पाये हैं? एक खयाल पाल पाये हैं? या कम से कम एक-दूसरे के सही दोस्त बन पाये हैं? एक-दूसरे के आगे ईमानदार रह सके हैं? एक-दूसरे के लिए सच्ची मुहब्बत जगा पाये हैं? अब बाँदा में मिल कर कौन-सी प्रगति छाँटोगे? तुम जाओ, और सारे समाचार मुझे दो। काफी होगा।
स्वयं प्रकाश के बारे में विस्तृत जानकारी तुमने दी, अच्छा किया। उनका एक-डेढ़ हफ्ता पहले एक पत्र आया था, तत्काल ‘क्यों’ के लिए कहानी भेजने का आग्रह करते हुए। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया है। वह इसलिए कि उन्होंने एक बार लिखा था कि उनका ‘क्यों’ से कोई सम्बन्ध नहीं है। और अब फिर कहानी माँग रहे हैं। अजीब मजाक है। पहले, ‘क्यों’ का समाचार पाकर, उत्साहित हो कर, एक गरीब व्यक्ति के महत्त्वपूर्ण, ईमानदार प्रयासों को उत्साहित करने के लिए मैंने तत्काल बतौर चंदा उन्हें 8 रुपये भेज दिये थे। मैं सोच रहा हूँ, मैंने गलती कर दी है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं।
‘समांतर’ को लेकर तुम्हारी सोच मिली। ठीक है। रमेश, मैं अब भी तहे दिल से चाहता हूँ कि समांतर हम लोगों का ठीक मंच बने। उसके जरिये हम लोग महत्त्वपूर्ण काम करें। देखो क्या होता है। मैं चाह रहा हूँ कि संभव हुआ, तो एक बार बंबई हो आऊँ। कमलेश्वर जी से, जितेन्द्र से और लोगों से मिल कर बात तो करें। देखें, कौन क्या सोच रहा है। जहाँ तक जितेन्द्र की बात है, उसे कोई क्या कह सकता है। वह खुद समझदार है। खुद सोच सकता है कि उसके लेखक और व्यक्ति की अधिक से अधिक रक्षा के लिए उसे कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिए। हम कुछ कहें, तो हो सकता है, उससे कई जगहों में कई तरह की गलतफहमी सिर उठाये।
रमेश, मैं बेहद अजीब-सी स्थिति से गुजर रहा हूँ। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, रमेश, हर दृष्टि से। इस नौकरी से भी तंग आ गया हूँ। किसी भी वक्त छोड़ दूँ। मगर, मेरे यार, यह बताओ, उसके बाद बीवी-बच्चों को कैसे पालूँ? क्या तुम कोई रास्ता दिखा सकोगे? दिखा सको, तो लिखो। मेरा लिखना-पढ़ना सब समाप्त होता जा रहा है इस माहौल में रह कर।
सारी बातें विस्तार से लिखो।
भाभीजी को प्रणाम। अरे, मैं अपनी बहूरानी को कैसे भूल सकता हूँ। जब राहुल तंग करता है, तो उसकी माँ कहती रहती है कि तुझे अपनी बीवी के पास दिल्ली भेज दूँगी, जो तुझे सुधार लेगी। मैं अगले पत्र के साथ तुम्हारे दामाद का चित्र भेजूँगा।
तुम्हारा
शरीफ
इसके बाद हमारा पत्राचार दो-चार संक्षिप्त पत्रों से अधिक आगे नहीं बढ़ सका। वह फिर कभी दिल्ली भी नहीं आया। यदि आया भी होगा, तो मुझसे मिला नहीं। सुधीर चौहान और जे. एल. रेड्डी जैसे अपने पुराने मित्रों से भी उसने लगभग नाता तोड़ लिया था। उसके जीवन के अंतिम चार वर्ष किस अवस्था में गुजरे, हम में से कोई नहीं जान सका। 1977 में हुई उसकी असामयिक मृत्यु पर सुधीर और रेड्डी मद्रास गये थे और उसके परिवार से मिल कर आये थे। मगर वे भी मुझे इतना ही बता सके कि शरीफ के अंतिम दिन बड़े आर्थिक कष्ट में गुजरे। वह बहुत अकेला और शायद अवसादग्रस्त भी हो गया था। शायद यही चीज उसकी अचानक हुई असामयिक मृत्यु का कारण बनी।
(पहल-106 से साभार)
सम्पर्क-
डॉ. रमेश उपाध्याय
107, साक्षरा अपार्टमेंट्स,
ए-3, पश्चिम विहार,
नयी दिल्ली-10063
मोबाईल – 09818244708